बदल देंगे आपके सोचने का तरीका Good Thoughts in Hindi शुभ विचारों में इतनी शक्ति होती है कि इससे आपका पूरा दिन Energetic हो सकता है | यदि मनुष्य अपने मन की गहराइयों में जाए और अपनी शक्तियों को पहचाने तो वह असंभव कार्यों को भी संभव कर सकता है| इस ब्लॉग में कुछ सर्वश्रेष्ट विचार पेश कर रहे हैं जिनको यदि आओ ध्यान से पढ़ें और मनन करें तो निश्चित ही आपको सकारात्मकता का अहसास होगा|

शुभ विचार
मनुष्य विचारों का पुंज है। किसी भी व्यक्ति की पहचान कि वह सज्जन-दुर्जन, शिष्ट- अशिष्ट, साधु-असाधु, संयमी-असंयमी है, विचारों से ही की जा सकती है। यजुर्वेट में कहा गया है-” आ नो भद्राः क्रतवो यंतु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्रभिद्र: ।” इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि कल्याणकारी, विघ्नरहित, शुभफलप्रद विचार हमें सभी ओर से प्राप्त हों, जिससे आलस्य रहित और रक्षा करने वाले देवता प्रतिदिन सदा हमारी समृद्धि करें। सद्रविचार हमें चारों ओर से प्राप्त हों। शास्त्रों में कहा गया है- ‘बालादापि शुभषितम्’ – अर्थात बालक से भी अच्छी बात ग्रहण करनी चाहिए।
मनुष्य जो कुछ मन में सोचता है वही वाणी से कहता है, वैसा ही कर्म करता है, उसी प्रकार बन जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है- “समानो मंत्रः समितिः समानं मनः सह चित्तमेषाम्” इस मंत्र का आशय यह है कि परमात्मा ने सभी को समान सुविधाएं दी हैं और समान उपकरण दिए हैं।मनुष्य का कर्तव्य है कि उसे दी गई सुविधाओं का समुचित प्रयोग करते हुए उन्नति करें। इसके लिए विचारों की एकता व भावनाओं का समन्वय आवश्यक है। अथर्ववेद के मंत्रों के माध्यम से कहा गया है कि लक्ष्य की पूर्ति के लिए हृदय की एकता अनिवार्य है तथा संकल्प, विचार और उद्देश्य भी समान होना आवश्यक है।
समाज को सुसंगठित करने के लिए समान विचार, समान कर्म और समान लक्ष्य, इन तीन तत्वों की आवश्यकता होती है। यह भावना सद्रविचारों से ही आ सकती है। शुभ विचारों से ही एक-दूसरे के हित-चिंतन की भावना उत्पन्न कर समाज के उत्थान के लिए प्रयत्नशील हुआ जा सकता है। मनुस्मृति के अनुसार जल से शरीर शुद्ध होता है। विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होती है।
हम शरीर के साथ-साथ मन, आत्मा व बुद्धि को शुद्ध रखेंगे तो हमारे विचार स्वतः ही शुभ हो जाएंगे। मानव-जीवन अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए है। अभ्युदय का अभिप्राय है-सांसारिक उन्नति, सांसारिक सुख व वैभव । निःश्रेयस का अर्थ मोक्ष के सुख से है। मनुष्य का मन शुभ विचारों से युक्त होने पर व्यक्ति आनंदित होता है। मनुष्य के उत्थान में विचारों का अत्यंत महत्व है। उत्तम व शुभ विचार मनुष्य को निरंतर प्रगति के मार्ग पर ले जाते हैं।

जीवन दिशा का ज्ञान
एक नदी को बहने के लिए दो किनारों की आवश्यकता होती है। बाढ़ तथा बहती हुई नदी में यह अन्तर है कि नदी का पानी एक- विशेष दिशा में बहता है, जबकि बाढ़ की अवस्था में पानी दिशाविहीन होकर बहता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि ऊर्जा को कोई दिशा नहीं प्रदान की जाती, तो यह दिग्भ्रमित हो जाती है।
जीवन की ऊर्जा के प्रवाह के लिए एक दिशा की आवश्यकता होती है। जब तुम प्रसन्न होते हो तो तुम्हारे अंदर अत्यधिक जीवन ऊर्जा होती है, लेकिन जब जीवन ऊर्जा नहीं जानती है कि कहां और कैसे जाना है, तब यह अवरुद्ध होकर जड़ हो जाती है। एक विद्यार्थी किसी स्कूल या कॉलेज में एक वचनबद्धता के साथ प्रवेश लेता है। तुम डॉक्टर के पास वचनबद्धता के साथ जाते हो कि डॉक्टर जो कुछ उपचार बताता है, उसको सुनते हो या उसके द्वारा दी गई औषधि को लेते हो। सरकार भी इसी तरह कार्य करती है।
एक परिवार भी वचनबद्धता के साथ चलता है। पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ वचनबद्ध है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में चाहे वह प्यार हो या व्यवसाय, मित्रता हो, वचनबद्धता अवश्य होती है। तुम किसी से किसी प्रकार की वचनबद्धता की आशा रखते हो और जब वे नहीं करते हैं तो तुम मानसिक हलचल से ग्रसित हो जाते हो। जब कोई अपनी वचनबद्धता का पालन नहीं करता, तो भी तुम मानसिक हलचल से ग्रसित हो जाते हो। लेकिन तुम देखो कि तुमने अपने जीवन में कितनी वचनबद्धताओं को लिया और उनका पालन किया है।
हमारी शक्ति, क्षमता या कार्यकुशलता हमारी वचनबद्धता के समानुपाती होता है। यदि तुम अपने परिवार का पालन-पोषण करने की वचनबद्धता लेते हो, तो तुम्हें उतनी शक्ति या क्षमता प्राप्त होती है। यदि तुम्हारी वचनबद्धता किसी समुदाय के प्रति है, तो तुम्हें उतनी अधिक मात्रा में शक्ति, प्रसन्नता और क्षमता प्राप्त होती है।
जितनी अधिक वचनबद्धता का तुम वहन करते हो, उतनी ही अधिक शक्ति तुम्हें उस वचनबद्धता का वहन करने के लिए प्राप्त त होती है। छोटी प्रतिवद्धता तुम्हें घुटन देती है, क्योंकि तुम्हारी क्षमता बहुत अधिक है, है, लेकिन तुम छोटे से छिद्र में फंसे हुए हो। जब तुम्हारे पास दस कार्य करने के लिए होते हैं और यदि एक कार्य गलत हो जाता है, तो तुम बाकी कार्यों को करते रह सकते हो। लेकिन, यदि तुम्हारे पास केवल एक हो कार्य करने के लिए होता है और वह अगर गलत हो जाता है तो तुम उसी से चिपके रह जाते हो।
तुम जितना ही बड़ा कार्य करने की वचनबद्धता करोगे, उतने ही बड़े स्रोत स्वयंमेव ही प्राप्त हो जाएंगे। जब तुम्हारे अंदर किसी कार्य को करने का विचार आता है, तो जब भी और जितना भी आवश्यक होता है उसके लिए स्त्रोत तुमको मिल जाते हैं। जो तुम कर सकते हो, उसको करने में तुम्हारा कोई विकास नहीं होता। अपनी क्षमता के बाहर हाथ-पैर फैलाने से तुम्हारा विकास होता है। यदि तुममें अपने शहर की देखभाल करने की क्षमता है और तुम यह कार्य करते हो, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन यदि तुम इसको और अधिक विस्तृत करते हुए अपने पूरे प्रदेश की देखभाल करने की वचनबद्धता करते हो, तो तुम्हें उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त होती है। जैसे ही तुम और अधिक उत्तरदायित्व लेते हो, तुम्हारी क्षमता बढ़ जाती है एवं तुम दैविक शक्ति के साथ एकीकृत हो जाते हो। जिस किसी भी क्षमता में तुम अपने समाज, पर्यावरण और इस प्रकृति के लिए कुछ करते हो, उतना ही तुम्हारे अन्दर भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता है। तुम्हारा हृदय इस अनुभव के साथ खुल जाता है कि तुम हर एक का हिस्सा हो।
संकल्प और संयम
Good Thoughts in Hindi
सोद्देश्य जीवन के लिए तन और मन, दोनों का संयम मूलाधार है। इसके बिना न तो जीवन का विकास संभव है और न लक्ष्य की उपलब्धि । बिना संयम का जीवन पाल चंपू रहित नौका की तरह असंभावनापूर्ण है, क्योंकि संयम से शक्ति मिलती है। संयम के लिए संकल्प की दृढ़ता वांछनीय है। संकल्प के लिए इच्छाशक्ति का अभ्यास आवश्यक है। संकल्पित व्यक्ति एकनिष्ठता चाहता है। वैज्ञानिक एडिसन, आर्कमिडीज, भक्त भोरा और तुलसी की तरह वह अपनी साधना के प्रति समर्पित रहता है। कला की साधना भी किसी कलाकार को संयमित और नियमित बना देती है।
इंद्रियों के सबम के लिए मन ऐसा केंद्र है जिससे संचालन एवं प्रवर्तन किया जाता है। महात्मा गांधी के तीन बंदरों के विषयों में यह कहा जाता है कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। इनमें वाणी का संयम बहुत महत्वपूर्ण है। गणेशजी ने संपूर्ण महाभारत का आलेखन किया, व्यास जी बोलते गए। इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर व्यास जी ने पूछा, ‘आप बोले क्यों नहीं।’ गणेश जी ने कहा, ‘यह वाणी है जिसका प्रभाव तत्क्षण पड़ता है, अनुकूल भी प्रतिकूल भी।’ अतः शब्द संभालकर बोलने की, सीख दी गई है।
आवेग रहित वाणी अनियंत्रित नहीं होती। ऐसी वाणी को तप की संज्ञा दी गई है। नीतिकार ने कहा है, ‘कम खाना, गम खाना, न हकीम के यहां जाना, न हाकिम के ।’ काम को नियंत्रित करने के लिए मन को वश में करना चाहिए जिसके लिए ब्रह्मचर्य- पालन बहुत आवश्यक है। बिना संयम के ब्रह्मचर्य की अवधारणा संभव नहीं। अध्यात्म कहना है जो लक्ष्मी चाहते हैं उन्हें लक्ष्मी की ही नहीं विष्णु की भी आराधना करनी चाहिए अन्यथा लक्ष्मी बिना विष्णु के नहीं रहतीं। साधक को संयम के लिए सतोगुणी होना चाहिए। उसके आहार, विहार, विचार और संकल्प में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।
रबड़ की तरह तानने पर ही मन अपने वश में रहता है और ढिलाई होने पर तुरंत यथास्थिति में लौट आता है। अतः संयम चाहे जितना पुराना हो, क्षणिक शिथिलता से टूट जाता है। संकल्प करना कल्पवृक्ष की तरह वरदानी होता है। संकल्प के लिए कठोर साधना चाहिए जिसे संयम का सातत्य पूर्ण करता है। संकल्प से प्रारंभ हुई यात्रा संयम से आगे बढ़ती है और सफलता तक पहुंचाती है।
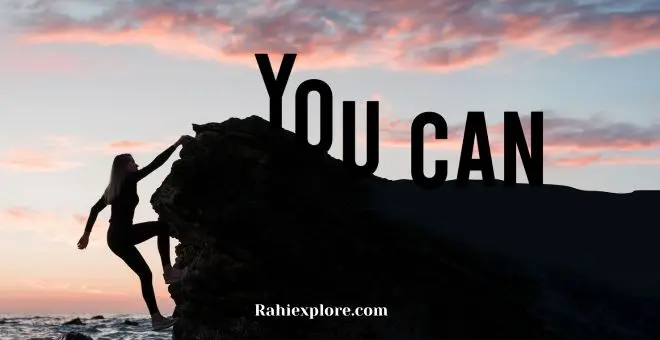
जीवन का आनंद
जीवन जीने का मार्ग संघर्षों से होकर गुजरता है। यह संघर्ष सुख और दुःख का है। मनोनुकूल परिस्थितियों को सुख और विपरीत परिस्थितियों को दुःख कहते हैं। वास्तव में दुःख और सुख अनुभव की चीजें हैं। एक ही परिस्थिति जो कभी सुख देती है वह कभी दुःखदायी भी हो जाती है। आनंद इससे ऊपर की चीज है। सुख-दुःख का संबंध मन और शरीर से होता है, जबकि आनंद का संबंध अंतरात्मा से होता है। आनंद अगर एक बार मिल गया तो व्यक्ति उसे छोड़ना नहीं चाहता। प्रश्न यह है कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो ? इसके लिए हमें स्वयं से प्रेम करना और दूसरों में प्रेम बांटना होगा।
ईश्वर द्वारा निर्मित जीवों के प्रति प्रेम करके हम आनंद प्राप्ति के पथ पर बढ़ सकते हैं। यशाशक्ति दूसरों की सेवा, सबके प्रति स्नेह, दया, सहानुभूति, परोपकार की भावना रखना और ईश्वर के प्रति समर्पणभाव रखना ही सच्ची मानवता है। जब तक हम सही अर्थों में मानव नहीं बन जाते तब तक आनंद की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम स्वयं सच्चे अर्थों में मानव बन जाएं तो जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी ही नहीं। यदि कभी हम एकांत में शांतचित्त बैठकर चिंतन और मनन करें तो जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रूप से सामने दिखाई देगा। हम संसार में क्यों आए हैं? कहां जाएंगे ? किसने भेजा है ? आदि अनेक प्रश्नों के उत्तर हमें स्वतः प्राप्त होंगे।
सामान्यतया हम जो भौतिक जीवन जी रहे हैं, यह जीना नहीं है। जीवन जीना एक कला है। इसके लिए ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक दिया है। सजग रहने वाला ही मुक्तिपथ पर आगे बढ़ सकता है। यह जीव ब्रह्म का अंश है। संसार में आकर वह अपने अस्तित्व को भूल गया है।
उसे उसके अस्तित्व का ज्ञान सद्गुरु कराता है। जब ज्ञान हो गया तो जीव उसी ब्रह्म में समाहित होने के लिए छटपटाता है। गुरु-कृपा से वह जान जाता है कि ‘मैं वही हूं’। जब यह अनुभव हो गया तो जीव चिल्ला उठता है- शिवोऽहम् शिवोऽहम्। जिस क्षण ऐसा अनुभव अंतरात्मा में हुआ उस दिन जो आनंद प्राप्त होगा वही परमानंद है। इस स्थिति में पहुंचकर भूख, प्यास, नींद, मान-अपमान, यश-अपयश और पाप-पुण्य आदि की चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। चारो तरफ आनंद ही आनंद। न पाने की इच्छा और न खोने का दुःख ।

